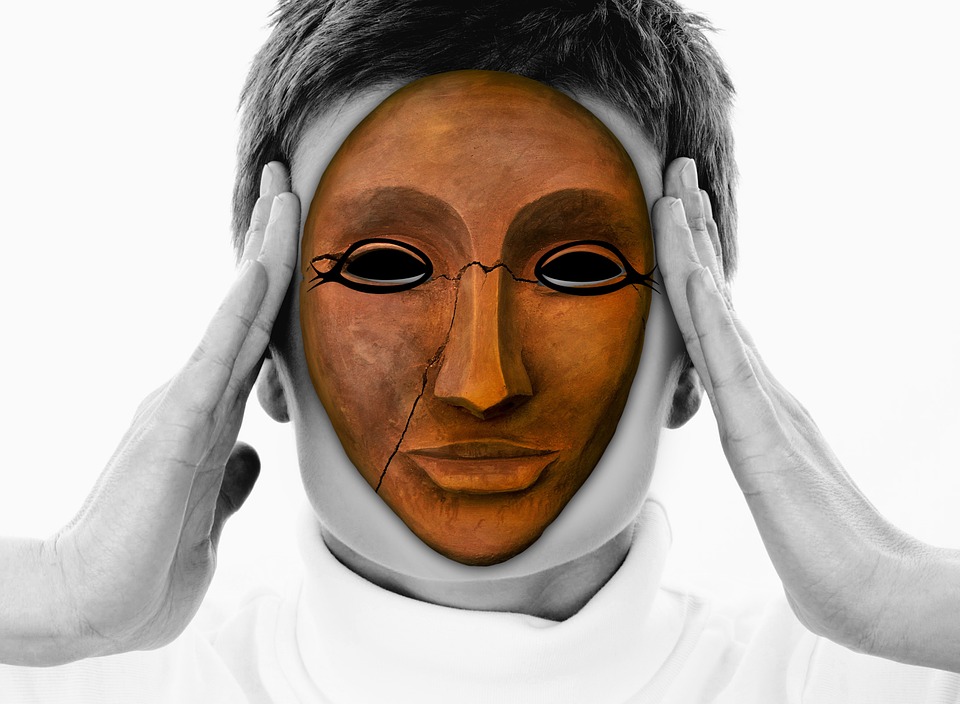# तिरंगे से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्रायः उपलब्ध नहीं है। सबसे रोचक बात यह है कि इसमें वास्तव में चार रंग हैं। तीन मुख्य रंगों का, भारतीय मानक ब्यूरो और अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार पूरा वर्णन है-भारतीय केसरी, श्वेत और भारतीय हरा। चौथा रंग हैं-गहरा नीला जिसमें तिरंगे की श्वेत पट्टी पर अशोक चक्र अंकित किया गया है, जिसमें 24 धूरियां हैं, भारत की सतत उन्नति का द्योतक, और इसमें भरा गहरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा इंगित करता है-ऊपर असीमित नीला गगन और नीचे गहरा नीला वरुण।
# 22 जुलाई 1947 को जब पंडित नेहरु ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रुप में अपनाने का प्रस्ताव रखा तो संविधान सभा के सामने दो झंडे, एक सूती खादी का और दूसरा रेशमी खादी का, प्रस्तुत किए गए थे। उनमें से सूती खादी का झंडा तो आज भी कानपुर स्थित सूती कपड़ा व पात्र निरीक्षणालय में मुहरबंद है, रेशमी खादी के झंडे का कुछ पता नहीं।
# आम धारणा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लाल किले की प्राचीर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा 15 अगस्त को फहराया था, पर यह सच नहीं है। उस दिन प्रातः 0830 बजे वायसराय भवन में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रुप में लाॅर्ड माउंट बैटन ने शपथ ग्रहण किया और फिर 1030 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, तत्पश्चात् काउंसिल हाउस(वर्तमान संसद भवन) पर तिरंगा फहराया गया। फिर शाम को पहला सार्वजनिक झंडारोहण समारोह युद्ध-स्मारक इंडिया गेट के पास प्रिंसेज पार्क में संपन्न हुआ। इस तरह उस दिन लाल किले पर झंडा फहराने का समय ही नहीं था। लाल किले पर तिरंगा 16 अगस्त 1947 को प्रातः 0830 बजे फहराया गया।
# 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो सारे देश में सार्वजनिक स्थलों और भवनों पर यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा फहरा दिया गया था, पर देश का एक ऐसा भू-भाग भी था जहां लगभग नौ सालों तक यह पता ही नहीं चला कि देश आजाद हो चुका है। लक्षद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण -मिनीकॉय द्वीप पर बने 47 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ पर युनियन जैक 02 अप्रैल 1956 तक फहराता रहा।
# भारतीय नौसेना और थल सेना ने 16 दिसंबर 1961 को गोआ, दमन और दीव को पुर्तगाली सरकार के कब्जे से मुक्त करा वहां पहली बार तिरंगा फहराया था।
इसी तरह पांडिचेरी में पहली बार 21 अक्तूबर1954 को तिरंगा पहली बार तब फहराया गया जब फ्रांसीसी सरकार ने समर्पण-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इसके पहले 02 अगस्त 1954 को दादरा-नागर हवेली को लोकशक्ति ने पुर्तगाली सत्ता से मुक्ति दिला वहां तिरंगा फहराया था।
# 26 जनवरी 1950 को भारत जब एक गणतंत्र बना तो भारत के राष्ट्रपति का एक निजी ध्वज बनाया गया जिसमें चार बराबर आयतें बनीं थीं। पहली और चौथी आयत नीले रंग की थी तो दूसरी ओर तीसरी लाल रंग की। पहली में राष्ट्रीय चिह्न अंकित था, दूसरी में हाथी, तीसरी में तराजू तो चौथी में एक छोटे कलश में अधखिले कमल का फूल अंकित था। यह ध्वज राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति की सवारी पर लगाया जाता था। इसी प्रकार राज्यों के राजप्रमुखों के भी अपने अपने निजी ध्वज थे जिनमें केसरी पृष्ठभूमि पर बादामी रंग में अशोक चिह्न अंकित था और नीचे राज्य का नाम लिखा होता था। सन् 1971 में जब प्रिवी पर्स समाप्त हुआ तो सभी भूतपूर्व देसी राज्यों के शासकों पर अपने अपने राज्यों के झंडे न फहराने का प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी समय से राष्ट्रपति और राज्यपालों-उपराज्यपालों ने भी निजी ध्वजों के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया।
# जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 370 के कारण अगस्त 2019 तक अपवाद था। वहां तिरंगे के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर का अपना हलधर लाल ध्वज फहराया जाता था; दिल्ली स्थित कश्मीर भवन पर भी यह देखा जा सकता था। पर 05-06 अगस्त 2019 को संसद के दोनों सदनों में बहुमत से और राष्ट्रपति के आदेश संख्या 273 से धारा 370 को पूरी तरह खतम कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन ऐक्ट पारित कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए। यह पुनर्गठन 31 अक्टुबर 2019 से लागू हुआ और अब जम्मू व कश्मीर का कोई अपना ध्वज नहीं है।(संपादित)
# 29 मार्च 1953 को जब शेरपा तेनजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो तिरंगे को युनियन जैक और नेपाल के झंडों के साथ विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर फहराया गया। अब तक पर्वतारोहियों द्वारा माउंट एवरेस्ट पर यह दस-ग्यारह बार फहराया जा चुका है।
# हमारा यह तिरंगा 1971 में अपोलो-15 के साथ संयुक्त राज्य अमरीका और कुछ अन्य देशों के ध्वजों के साथ पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया। 1984 में यह विंग कमांडर राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टंग कर गया।
# 09 जनवरी 1982 को जब भारतीय अंटार्कटिका अभियान पहली बार दक्षिण गंगोत्री पहुंचा तो वहां तिरंगा फहराया गया। दक्षिण ध्रुव पर कर्नल जे के बजाज ने इसे 17 जनवरी 1981 को पहली बार फहराया। 28 सितंबर 1985 को कर्नल पी पी चौधरी ने इसे अपनी नौका ‘तृष्णा’पर फहरा कर पूरे विश्व की समुद्री यात्रा करा दी और 10 जनवरी 1987 को भारत लौटे। 30,000 नॉटिकल मील से भी अधिक की समुद्री यात्रा तिरंगे ने 470 दिनों में पूरी की।
# तिरंगा केवल हाथ से बने खादी के कपड़े का ही बनाया जाता है, चाहे वह सूती है या रेशमी, और इसे सिलने के लिए भी खादी का धागा ही प्रयोग किया जाता है। पूरे देश में एक ही जगह, बंगलोर-पूणे रोड पर ‘गरग’नाम के एक छोटे गांव में 1954 में स्थापित एक केन्द्र में ही यह कपड़ा बनाया जाता है। पर झंडों का निर्माण मुख्य रुप से दो तीन जगहों पर होता है- आॅर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई और तीसरा खादी ग्रामोद्योग दिल्ली। लेकिन निजी निर्माताओं द्वारा इसके निर्माण पर कोई रोक नहीं है। नियमत: हाथ से बने एक वर्गफुट के तिरंगे का वजन 250 ग्राम होना चाहिए।
# राष्ट्रीय ध्वज के विषय में एक और अल्पविदित तथ्य यह भी है कि इसके नौ मानक आकारों में पहला 21’x14′ देश के किस इमारत पर फहराया जाता होगा, बहुत पूछ-ताछ करने पर भी पता नहीं चला-क्योंकि लाल किले और राष्ट्रपति-भवन जैसे विशाल भवनों पर भी दूसरे नंबर का मानक आकार, अर्थात 12’x8’के ध्वज ही फहराने जाते हैं। एक सूचना के अनुसार इतने बड़े आकार का झंडा सारे देश में संभवतः केवल एक ही स्थान पर फहराये जाने की संभावना है और वह है मद्रास स्थित सेंट जाॅर्ज फोर्ट, जिस पर देश का सबसे ऊंचा सागवान (टीक वुड) का लकड़ी का ध्वज दंड (45.7 मीटर ऊंचा) लगा है।
# राष्ट्रीय ध्वज का सबसे छोटा मानक आकार, क्रम में नौवां-6″x4″ विदेशियों के साथ राजकीय सम्मेलनों और वार्ताओं के दौरान मेज पर रखने के काम आता हैं। इसे रेशम से बनाते हैं, जबकि दूसरे मानक आकारों के ध्वज सूती खादी के बने होते हैं।
# सरकारी भवनों पर तथा दूसरे अवसरों पर सूती खादी से बने झंडों का ही प्रयोग होता है, पर राष्ट्रीय गरिमा को ध्यान में रखकर 26 जनवरी को राजपथ पर (राष्ट्रपति द्वारा) और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर (प्रधान मंत्री द्वारा) जो ध्वज फहराये जाते हैं, वे रेशमी होते हैं।
# 1987 में आजादी की चालीसवीं वर्षगांठ पर राजधानी दिल्ली में चालीस हजार राष्ट्रीय ध्वज एक सप्ताह तक रात-दिन फहराने गए थे।
# प्रथानुसार सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, पर संसद भवन पर तीन राष्ट्रीय ध्वज हर रोज एक साथ फहराये जाते हैं, एक-एक ध्वज लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के लिए होता है। 1985 के पहले, जब सर्वोच्च न्यायालय भी संसद भवन में ही स्थित था, यहां एक साथ चार-चार राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते थे।
# केन्द्रीय सचिवालय के नाॅर्थ ब्लाॅक के विजय चौक की ओर स्थित बुर्जों पर भी एक साथ दो-दो राष्ट्रीय ध्वज फहराते जाते हैं। इसका कारण संभवतः अंग्रेजों के समय से चली आ रही परंपरा है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व यहां दो-दो यूनियन-जैक फहराए जाते थे, जिनके लिए बुर्जों पर दो-दो तिरछे ध्वज दंड विशेष रुप से लगे हुए हैं।
(भारतीय राष्ट्र ध्वज पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम लेखक लेफ्टिनेंट कमांडर के वी सिंह रचित “तिरंगे की गौरव गाथा” नामक पुस्तक से साभार)